नाग संस्कृति का अद्भुत संसार: एक विस्तृत अन्वेषण
सत्येन्द्र कुमार पाठक
साँप, एक ऐसा प्राणी है जो अनादि काल से मानव सभ्यता के साथ गहरे जुड़ाव में रहा है। भारत में तो यह संबंध और भी गहरा है, जहाँ साँपों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र, रहस्यमय और शक्तिशाली सत्ता के रूप में देखा जाता है। उनकी उपस्थिति पुराणों से लेकर लोककथाओं तक, रीति-रिवाजों से लेकर दैनिक जीवन तक फैली हुई है। यह आलेख साँपों के इस अनूठे और बहुआयामी संसार का विस्तृत अन्वेषण प्रस्तुत करता है
भारतीय परंपरा में अष्टकुली नागों की विशेष मान्यता है, जिनमें अनंत (शेष), वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कोटक और शंखपाल प्रमुख हैं। ये नाग विभिन्न दिशाओं, लोकों और कार्यों से जुड़े हुए हैं। संख्या कोष में नाग को आठ का पर्याय माना गया है, जो इस अष्टकुली अवधारणा को और पुष्ट करता है। 'अग्नि पुराण' में 80 प्रकार के विभिन्न नाग कुलों का वर्णन मिलता है। 'कथा सरित्सागर' नागों से संबंधित विस्तृत कथाएँ प्रस्तुत करता है।'नीलमत पुराण' में भी नागों से जुड़ी अनेक कहानियाँ , 'कूर्मपुराण' में सहअस्तित्व के प्रसंगों में नागों के महत्व को दर्शाया गया है।संतान प्राप्ति की कामना के लिए नागों का अर्चन किया जाता था।शिव कथाओं का विकास भी कहीं न कहीं इन प्राचीन नाग कथाओं की तर्ज पर हुआ प्रतीत होता है।
नाग योनि में पुनर्जन्म की मान्यता भी यह दर्शाती है कि नागों को आत्मा के चक्र से जुड़ा हुआ माना है।साँपों का प्रभाव केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक जीवन, परंपराओं और दैनिक व्यवहार में भी गहराई से समाया हुआ है। साँप ने मानव को बहुत कुछ सिखाया है। कपड़े बदलने की अवधारणा मानव ने सांप से सीखी, और कपड़ों का प्राचीन नाम "कंचुक" सांप की केंचुली से ही आया है। कबीलाई समाजों में, जब लोगों ने ज़मीन पर घर बनाना शुरू किया, तो साँपों से बचाव के लिए उनकी उतारी गई केंचुली को जलाया जाता था, क्योंकि साँप अपनी केंचुली से घृणा करता है।
संरक्षक और सखा - किसान के लिए साँप एक सखा और खेतों का रखवाला है, जो फसलों को चूहों और अन्य कीटों से बचाता है। इसीलिए उसे "भौमिया" (भूमि का देवता) मानकर पूजा जाता है और चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। यह प्रकृति और मानव के बीच के सहजीवी संबंध का प्रतीक है।
भारत ही नहीं, मिस्र, यूनान, कंबोडिया और जावा जैसे अनेक देशों में गाँवों, नगरों, जलाशयों और पहाड़ों के रास्तों में नागों की मूर्तियाँ या संकेतक मिलते हैं। इससे पता चलता है कि नाग मार्ग के सूचक और प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने प्राचीन यात्रियों को दिशा दिखाई होगी। नागों के अपने चिह्न भी थे, और हाथी, उरग, ताल, माल जैसे लगभग सौ वस्तुओं को नाग का पर्याय माना गया है, जो उनकी व्यापक उपस्थिति को दर्शाता है।
राजस्थान में गोगाजी, तेजाजी, देवजी, ताखाजी, गातोड़जी, और यहाँ तक कि कल्लाजी, जयमल जैसे लोकदेवता नाग योनि को प्राप्त माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। नाग पंचमी के दिन "ऊँ अष्टकुल नागनागेभ्यो नम:" मंत्र के साथ सर्पों की पूजा की जाती है, जो उनकी दैवीय स्थिति को पुष्ट करता है। असम प्रांत की 'नागा' जाति तो नाग देवता के समुद्रभूत होने का गर्व महसूस करती है।
चिकित्सा और रसायन - नागों को रसायन और अमृत साधक के रूप में भी जाना जाता था। आयुर्वेद में सीसे को "नाग" कहा जाता है, और नाग भस्म जैसी औषधियाँ पेट संबंधी बीमारियों और मधुमेह (प्रमेह) में प्रयोग की जाती हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में नागों से जुड़े तत्वों का गहरा ज्ञान था।
जनमेजय का नाग यज्ञ - द्वापरयुग में महाभारत में वर्णित जनमेजय का नाग यज्ञ एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें उन्होंने अपने पिता परीक्षित की सर्पदंश से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का संहार करना चाहा। ऋषि आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की, जिसके बाद यह मान्यता स्थापित हुई कि सर्प भय होने पर ऋषि आस्तिक का नाम लेने से सर्प वापस चला जाता ह
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन यमुना नदी से उसके परिवार को हटाकर किया गया था। यह कथा दर्शाती है कि कैसे संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तिशाली शक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है।
नागपाश प्राचीन युद्ध तकनीक थी जिसमें नागों का प्रयोग शत्रु को बांधने के लिए होता था। रामायण के लंकाकांड में इसका वर्णन मिलता है, जहाँ मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया था, जिसे गरुड़ ने ही भेद सका। अथर्ववेद में भी इसका प्राचीन वर्णन मिलता है। यह एक प्रकार की "माया विद्या" थी और मध्यकाल में इस पर अधिक विश्वास किया जाता था।
ज्योतिष में कालसर्प दोष की मान्यता है, जहाँ ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातकों को नागपाश या कालसर्प दोष में बंधा हुआ माना जाता है। इसकी निवृत्ति के लिए नागों की पूजा का विशेष विधान है।
नागदा और नागपुर नागों ने तक्षशिला, नागपुर, नागौर, अहिच्छत्रपुर जैसे कई नगर बसाए थे, जो एक विस्तृत नागलोक का हिस्सा थे। मेवाड़ में नागदा कभी गुहिलों की राजधानी था, और एकलिंग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ये स्थान नाग सभ्यता की व्यापकता के प्रमाण हैं।गंध और साँपों की मान्यताएँ - लोक मान्यताओं में गंध का उपयोग साँपों को दूर रखने या आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"इसरगत" की गंध: मिथिला में "इसरगत" नामक एक पौधे की लकड़ी या जड़ को कलाई पर बांधा जाता था। माना जाता था कि इसकी विशेष गंध के कारण साँप इसके नजदीक नहीं आते। यह एक प्राचीन अंधविश्वास न होकर, बल्कि प्राकृतिक रूप से साँपों को दूर रखने का एक पारंपरिक ज्ञान हो सकता है।
लहसुन और फिनायल: बराक घाटी जैसे क्षेत्रों में लहसुन के घोल का छिड़काव साँपों, खासकर खतरनाक अलोध (कोबरा की एक प्रजाति) को दूर रखने के लिए किया जाता है। घरों के आसपास फिनायल का उपयोग भी इसी उद्देश्य से होता है, हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर बहस हो सकती है।तेजपत्ता और अन्य सुगंध: चूहों को भगाने के लिए तेजपत्ता जलाकर धुआँ करना, या कुत्ते को रोकने के लिए पानी की बोतल में नील भरकर रखना भी गंध के इसी अनुप्रयोग को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन समाजों में प्रकृति के साथ सहअस्तित्व बनाए रखने के लिए गंध और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग एक महत्वपूर्ण तरीका था।
वेद में सर्प शब्द के दार्शनिक अर्थ - वेद में सर्प शब्द के कई गहरे और दार्शनिक अर्थ दिए गए हैं, जो केवल भौतिक सरीसृप से कहीं परे हैं: आकाशीय आयाम: वेद में सर्प को आकाश का आठवां आयाम माना गया है। इसे वृत्र, अहि या नाग भी कहा गया है। यह भौतिक विश्व के पाँच आयामों (रेखा, पृष्ठ, आयतन, पदार्थ, काल) के परे, चेतना और संबंध के उच्चतर आयामों को दर्शाता है। वृत्र को वह शक्ति माना गया है जो सभी को घेरती है, जो ब्रह्मांडीय सीमाओं का प्रतीक है।आकाशगंगा की सर्पाकार भुजा: अहिर्बुध्न्य (ब्रह्मांड में द्रव जैसे फैले पदार्थ में सर्प जैसी भुजा) आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं को दर्शाता है। पुराणों का शेषनाग इसी का प्रतीक हो सकता है, जिसके 1000 सिर हैं और पृथ्वी उसमें एक कण के समान स्थित है।पृथ्वी की वक्र सतह: पृथ्वी को स्वयं सर्पराज्ञी कहा गया है, जिसकी वक्र परिधि एक सर्प के समान है। सात द्वीपों को जोड़ने वाले आठ दिङ्नाग इसी अवधारणा को बल देते हैं।व्यापार और मार्ग: समुद्री यात्रा के मार्गों को नाग वीथी कहा गया है, जो प्राचीन काल में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। व्यापारिक वस्तुएँ परिवहन करने वाले लोगों को भी नाग कहा गया है।पूजा का महत्व: नाग पूजा को पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले मनुष्य रूप नागों के कार्य में सहयोग के लिए शक्ति देना माना गया है, ताकि वे विश्व का भरण-पोषण कर सकें। इसे देवताओं द्वारा दिया गया आज्य (घी) कहा गया है, जिसका स्रोत दूध है।नक्षत्रों से संबंध: आश्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। यह नक्षत्र ब्रह्मांड की सर्पिल भुजा के मध्य में स्थित है। श्रावण मास में जब सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में रहता है (शुक्ल पंचमी के निकट), तब नाग पूजा की जाती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा इसके विपरीत श्रवण नक्षत्र में होता है, जिसका देवता गरुड़ है, जो सांप का विपरीत है।नाग भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समाजों तक, हर संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल एक जीव नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान, पुनर्जन्म, चिकित्सा, संरक्षण और यहां तक कि विनाश का भी प्रतीक है। इसका महत्व भौगोलिक सीमाओं से परे है, और विभिन्न संस्कृतियों में इसके विशिष्ट अर्थ और भूमिका है।
नागों की उत्पत्ति और उनके माता-पिता के संबंध में विस्तृत वर्णन मिलता है।नागों के पिता: पौराणिक कथाओं के अनुसार, नागों के पिता महर्षि कश्यप हैं। वे सप्तर्षियों में से एक थे और प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र भी माने जाते हैं। महर्षि कश्यप की कई पत्नियाँ थीं, जिनसे विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई।नागों की माता: नागों की माता का नाम कद्रू है। वे दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से एक थीं और महर्षि कश्यप की तेरह पत्नियों में से एक थीं। कथाओं के अनुसार, कद्रू ने महर्षि कश्यप से एक हजार तेजस्वी नाग पुत्रों का वरदान माँगा था। इसी वरदान के परिणामस्वरूप, कद्रू ने अंडे दिए जिनसे बाद में सभी नागों की उत्पत्ति हुई। इनमें शेषनाग, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक जैसे प्रमुख नाग शामिल थे। पुराणों के अनुसार कद्रू और उनकी बहन विनता (जो पक्षीराज गरुड़ की माता थीं) के बीच एक घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लगी थी। कद्रू ने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ को काला दिखाने के लिए उस पर लिपट जाएँ। जब नागों ने ऐसा किया और कद्रू शर्त जीत गईं, तो उन्होंने विनता को अपनी दासी बना लिया। कुछ नागों ने अपनी माता के इस छल का विरोध किया, और इसी कारण कद्रू ने उन्हें जनमेजय के सर्पयज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था ।
पौराणिक शासन: भारत में नागों ने केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि शाब्दिक रूप से भी कई क्षेत्रों पर शासन किया है। प्राचीन काल में नागवंशों का अस्तित्व था, जिनके सिक्के पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं। तक्षशिला, नागपुर, नागौर, अहिच्छत्रपुर, पद्मावती (पवाया), मथुरा, विदिशा और कान्तिपुरी राजधानियाँ नागों से संबंधित थीं।
सांस्कृतिक प्रभाव: भारतीय संस्कृति में नागों को दिव्य प्राणी, संरक्षक और उर्वरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान शिव के आभूषण, भगवान विष्णु की शैय्या और कई लोक देवताओं जैसे गोगाजी, तेजाजी आदि से जुड़े हैं। नाग पंचमी का त्योहार विशेष रूप से नागों की पूजा के लिए समर्पित है।पारिस्थितिक महत्व: भारतीय ग्रामीण समाज में नागों को "खेतों का रखवाला" या "क्षेत्रपाल" माना जाता है, क्योंकि वे चूहों और अन्य कीटों का भक्षण कर फसलों की रक्षा करते हैं। यह दर्शाता है कि पारंपरिक समाजों ने नागों के पारिस्थितिक संतुलन में योगदान को समझा था।राजसत्ता और सुरक्षा: प्राचीन मिस्र में साँपों को राजसत्ता, सुरक्षा और देवत्व का प्रतीक माना जाता था। फिरौन (राजाओं) के मुकुट पर अक्सर खड़े कोबरा का चित्र होता था, जिसे उरायस (Uraeus) कहा जाता था, जो शाही शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था।दैवीय भूमिका: साँप देवी वजएट निचले मिस्र की संरक्षक देवी थीं, जिन्हें अक्सर कोबरा के रूप में चित्रित किया जाता था। विशाल सर्प एपेप अंधकार और अव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, जो हर रात सूर्य देवता रा को निगलने की कोशिश करता था।आइसिस देवी: मिस्र में एक नागदेवी या नागिन थी जिसे आइसिस के नाम से जाना जाता था। यह चंद्रमा की देवी मानी जाती थी और ओसीरिस-मिथक में एक प्रमुख देवी थ
चिकित्सा और उपचार: ग्रीक पौराणिक कथाओं में, चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस (Asclepius) की छड़ी पर लिपटा साँप ज्ञान, चिकित्सा और उपचार का प्रतीक है। यह प्रतीक आज भी विश्वभर के चिकित्सा संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। साँप की केंचुली छोड़ने की क्षमता को नए जीवन और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था।
रहस्यमय और भयावह: ग्रीक मिथकों में मेडूसा (Medusa) जैसी आकृतियाँ भी थीं, जिनके बाल साँप थे और उन्हें देख लेने से व्यक्ति पत्थर बन जाता था, जो साँप के भयावह और रहस्यमय पहलू को दर्शाता ह सृष्टि और बुद्धि: चीनी पौराणिक कथाओं में, मातृ देवी नुवा (Nuwa) को आधा साँप के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने मिट्टी से मनुष्यों की रचना की थी। साँप को चीनी राशि चक्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जहाँ इसे बुद्धिमान, आकर्षक, रहस्यमय, चतुर और रूपांतरण व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 2025 को "ईयर ऑफ द स्नेक" घोषित किया गया है, जो इस प्रतीक के महत्व को दर्शाता है।मेसो-अमेरिका (माया, एज़्टेक सभ्यताएँ) मेसो-अमेरिकी संस्कृतियों में, साँप को भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक द्वार माना जाता था। पंख वाले साँप-देवता: क्वेटज़ालको एक पंख वाले साँप-देवता थे, जो एज़्टेक और माया सभ्यताओं में एक प्रमुख देवता थे, जो सृष्टि, ज्ञान और हवा से जुड़े थे ।सृष्टि का रचयिता: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग रेनबो सर्प (Rainbow Serpent) को सृष्टि का रचयिता और पृथ्वी पर जीवन के स्रोत के रूप में मानते हैं। यह एक शक्तिशाली आत्मा है जो जल, जीवन और वर्षा से जुड़ी है।नॉर्स पौराणिक कथाएं: जॉर्नमुंगंदर (Jörmungandr), मध्यगामी सर्प, नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक विशाल समुद्री सर्प है जो विश्व को घेरे हुए है। अफ्रीकी धर्म: कई अफ्रीकी संस्कृतियों में साँपों को पूर्वजों, उर्वरता और उपचार से जोड़ा जाता है।
नागों का महत्व केवल उनकी धार्मिक या पौराणिक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अन्य आयामों को भी छूता है:पुनर्जन्म और कायाकल्प: साँप अपनी केंचुली उतारते हैं, जो पुनर्जन्म, नवीकरण और अनंत जीवन का एक शक्तिशाली प्रतीक है।ज्ञान और रहस्य: उनकी रहस्यमय प्रकृति, छिपा हुआ जीवन और कभी-कभी विषैला स्वरूप उन्हें ज्ञान, गुप्त विद्याओं और छिपी हुई शक्तियों से जोड़ता है।संरक्षण और विनाश: नाग एक साथ संरक्षक और विनाशक दोनों हैं। वे खेतों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उनका विष घातक भी हो सकता है। यह द्वैत प्रकृति उनके महत्व को और बढ़ाती है। शेषनाग और विश्व सर्प की अवधारणाएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था, स्थिरता और स्वयं ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतीक हैं। भारतीय योग और तंत्र में, कुंडलिनी शक्ति को रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडली मारे हुए साँप के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सुषुप्त ऊर्जा का प्रतीक है जिसे जागृत करने से आध्यात्मिक विकास होता है।
कालखंड: नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी (लगभग 64 ईस्वी) में हुई मानी जाती है। इसके संस्थापक फणीमुकुट राय थे। इस राजवंश ने सन् 1951 में जमींदारी प्रथा के अंत होने तक, लगभग 1,950 सालों तक शासन किया, जो इसे विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक बनाता है।
फणीमुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया, जिसे बाद में प्रताप राय ने चुटिया स्थानांतरित कर दिया। नागवंशी शासकों ने 1870 में अपनी राजधानी पालकोट से रातू स्थानांतरित की।नागवंशियों ने शुरू में मुंडाओं की शासन व्यवस्था में बिना बड़े बदलाव किए इसे संचालित किया और विस्तार दिया। उनकी अपनी सैन्य व्यवस्था भी थी, और राजाओं व जमींदारों के पास निजी सेनाएँ हुआ करती थीं। नागवंशी राजघराने के 62वें और अंतिम राजा लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव थे, जिनका निधन 2014 में हुआ। 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया।
उत्तराखंड में भी नागवंशी राजाओं का शासन रहा है, खासकर गुप्तकाल से पहले। नागपुर और गोपेश्वर: उत्तराखंड में नागवंशी राजाओं के राज्य की संज्ञा नागपुर को दी गई है, जिसकी राजधानी गोपेश्वर थी। यहाँ के त्रिशूल लेखों में नागवंशी राजाओं का उल्लेख मिलताहै।भारत में नागों का शासन और स्थिति - भारत में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र, रहस्यमय और शक्तिशाली सत्ता के रूप में देखा जाता है। उनका प्रभाव विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक रूप से रहा है।जम्मू-कश्मीर में नागों का गहरा संबंध है। कश्मीर की घाटी को प्राचीन काल में 'नाग-लोक' के रूप में जाना जाता था। यहां कई नाग झरने और नाग देवता के मंदिर पाए जाते हैं। कश्मीर के इतिहास में नागवंशी शासकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। शेषनाग झील, अनंतनाग और वेरिनाग जैसे स्थान नागों से जुड़े हुए हैं।कर्नाटक में नाग पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा है, खासकर तुलु नाडु (तटीय कर्नाटक) क्षेत्र में। यहाँ नागारधने (नाग पूजा) प्रचलित है। कई स्थानों पर नागबन (नागों के लिए पवित्र वन) और नाग मंदिर हैं। ऐतिहासिक रूप से, गंगा राजवंश और होयसल राजवंश के शासकों ने भी नागों के साथ अपने संबंध दर्शाए हैं।
नागालैंड का नाम ही 'नागा' जनजाति से आता है, जो स्वयं को नागों से संबंधित मानते हैं। उनकी पौराणिक कथाओं और लोककथाओं में नागों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही नागों और उनसे जुड़ी जनजातियों का गढ़ रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी प्राचीन नागवंशीय प्रभाव रहा है। इंद्रप्रस्थ के प्राचीन ग्रंथों में नागों का उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है कि पांडवों ने खांडव वन को जलाकर नागों को विस्थापित किया था। यद्यपि प्रत्यक्ष नाग शासकों का प्रमाण कम है, फिर भी पौराणिक संदर्भ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा विशेष रूप से नागों से जुड़ा हुआ है। मथुरा के नागवंशी शासकों का इतिहास प्रसिद्ध है। यहां कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन एक प्रमुख पौराणिक घटना है। अहिच्छत्रपुर (बरेली के पास) भी एक प्राचीन नाग राजधानी थी ।मध्य प्रदेश में पद्मावती (पवाया) और विदिशा जैसी जगहें नागवंशियों की राजधानियाँ रही हैं। यहां से प्राप्त सिक्के और शिलालेख नागों के शासन की पुष्टि करते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर नागों की पूजा पूरे राज्य में की जाती है।राजस्थान में भी नागवंशीय प्रभाव देखा जाता है। नागौर का नाम नागों से जुड़ा है। यहां के लोक देवता जैसे गोगाजी, तेजाजी और पाबूजी को नागों से संबंधित माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है।असम प्रांत की 'नागा' जाति स्वयं को नाग देवता के वंशज मानती है। यहां की लोककथाओं और आदिवासी परंपराओं में नागों का गहरा महत्व है।आंध्र प्रदेश में भी नागों की पूजा होती है, विशेषकर गाँवों में जहाँ उन्हें क्षेत्रपाल के रूप में देखा जाता है। प्राचीन काल में कुछ क्षेत्रों में नागवंशीय प्रभाव होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र में नागों को पवित्र माना जाता है। यहां कई नाग मंदिर हैं, और नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। विदर्भ क्षेत्र में प्राचीन नागवंशीय प्रभाव की बात कही जाती है।
ओडिशा के इतिहास में नागों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां के प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों में नागों के चित्रण मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ओडिशा में भी नागों से संबंधित शासक वर्ग मौजूद था।
बिहार और विशेष रूप से झारखंड में नागवंशी राजवंश का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। फणीमुकुट राय द्वारा स्थापित इस राजवंश ने सदियों तक शासन किया। इनकी राजधानियाँ सुतियाम्बे, चुटिया और रातू रहीं।
बंगाल में नागों से जुड़ी लोककथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। देवी मनसा (नाग देवी) की पूजा विशेष रूप से बंगाल में की जाती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में बंगाल के कुछ हिस्सों में नागों के प्रभाव का उल्लेख है। झारखंड में नागवंशी राजवंश सबसे प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने लगभग 1,950 सालों तक शासन किया। यह क्षेत्र नागों की पौराणिक कथाओं और लोक संस्कृति से गहरा जुड़ा हुआ है।गुजरात में नागों की पूजा प्रचलित है, और कई स्थानों पर नाग देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ प्राचीन नागवंशीय प्रभाव है।
पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों के कुछ हिस्से, जो प्राचीन भारत का हिस्सा थे, वहां भी नागों का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व रहा है। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण नाग राजधानी थी, जो अब पाकिस्तान में है। सिंध में सूफी परंपराओं में भी नागों का उल्लेख मिलता है। बांग्लादेश में भी देवी मनसा की पूजा प्रचलित है, जो नाग देवी हैं। यहां भी नागों से जुड़ी लोककथाएं और ग्रामीण परंपराएं मिलती है। अफगानिस्तान के कुछ प्राचीन क्षेत्रों में, जहां बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव था, नागों के चित्रण और कथाएं मिलती हैं। गांधार कला में नागों को अक्सर दर्शाया जाता था। प्राचीन फारसी (ईरानी) पौराणिक कथाओं में भी सर्पों या ड्रेगन का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अक्सर नकारात्मक या द्वेषपूर्ण शक्तियों के रूप में चित्रित किया जाता था, लेकिन कभी-कभी ज्ञान से भी जोड़ा जाता था।इंग्लैंड और आयरलैंड में प्राचीन सेल्टिक और नॉर्स पौराणिक कथाओं में सर्पों का प्रतीकात्मक महत्व रहा है, हालांकि वे भारतीय नागों से भिन्न हैं। यहां सर्पों को अक्सर सृजन, नवीनीकरण या रहस्यमय शक्तियों से जोड़ा जाता था।रूस और स्लाविक लोककथाओं में सर्पों और ड्रेगन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां सर्पों को अक्सर धन के संरक्षक या जादुई शक्तियों वाले प्राणी के रूप में देखा जाता है।थाईलैंड में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण नागों का अत्यधिक महत्व है। नागों को अक्सर बुद्ध के संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, और कई मंदिरों में नाग की मूर्तियों को देखा जा सकता है। मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी के कारण, नाग पूजा और नागों से संबंधित भारतीय परंपराएं यहां भी प्रचलित हैं।
श्रीलंका में नागों का गहरा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि बुद्ध की रक्षा एक नागराज ने की थी। श्रीलंका में नाग जनजाति के अस्तित्व की भी बात कही जाती है, जिन्होंने प्राचीन काल में द्वीप के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अरब (मध्य पूर्व) का सुमेरियन और बाबुलियन में भी सर्पों के चित्रण और प्रतीक मिलते हैं। इन्हें अक्सर सृजन, उर्वरता या चिकित्सा से जोड़ा जाता था ।इज़राइली (यहूदी) परंपरा में सर्प का उल्लेख अक्सर ईडन गार्डन की कहानी से जुड़ा है, जहाँ इसे धोखे और प्रलोभन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चिकित्सा के प्रतीक के रूप में भी सर्प का उपयोग मिलता यूरोप में, खासकर ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में, सर्पों का महत्व रहा है। ग्रीक चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस की छड़ी पर लिपटा साँप आज भी चिकित्सा का प्रतीक है। यूरोप में 'नाग' जैसे शासक वर्ग का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, बल्कि उनका महत्व प्रतीकात्मक या पौराणिक रहा है।नेपाल में नागों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारत के समान ही है। नाग पूजा और नाग पंचमी का त्योहार यहां भी धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में कई नाग मंदिर और नाग देवता से जुड़े स्थान हैं।
भूटान में भी बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण नागों को पवित्र माना जाता है। यहां की लोककथाओं और कला में नागों का चित्रण मिलता है।चीनी पौराणिक कथाओं में सर्पों और ड्रेगन का गहरा महत्व है। ड्रेगन को अक्सर शक्ति, सौभाग्य और शाही अधिकार का प्रतीक माना जाता है। मातृ देवी नुवा को आधा सर्प के रूप में दर्शाया गया है। चीनी राशि चक्र में भी साँप एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नागों का संसार वास्तव में अजूबा और अनूठा है। वे न केवल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विश्व की कई अन्य सभ्यताओं में गहरे रूप से समाए हुए हैं। उनकी कथाएँ, मान्यताएँ और प्रतीकवाद हमें प्रकृति के साथ हमारे जटिल संबंधों, आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान की गहराई को समझने में मदद करते है।
झारखंड का क्षेत्र, जिसे पहले दक्षिण बिहार का हिस्सा माना जाता था, नागवंशी शासकों का प्रमुख गढ़ रहा है।
उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र नागवंशी राजवंश का हृदय स्थल रहा है।राजा फणीमुकुट राय को नागवंशी राजवंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास ( 64 ईस्वी) इस राजवंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया। बाद में प्रताप राय ने इसे चुटिया स्थानांतरित किया, और अंततः राजधानी रातू (रांची के पास) में स्थापित हुई। नागवंशियों ने लगभग 1,950 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जब तक कि 1951 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हो गया। नाग राजवंश छोटानागपुर पठार के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था और इसने इस क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। बंगाल में देवी मनसा की पूजा का अत्यधिक प्रचलन सर्पों की देवी मानी जाती हैं। यह दर्शाता है कि नागों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व यहां गहरा रहा है। ओडिशा का प्राचीन राजवंशों,नागवंशी गंगों (पूर्वी गंग राजवंश) के साथ नागों का संबंध जोड़ा जाता है। यद्यपि वे स्वयं को सीधे नागों के वंशज नहीं मानते थे, उनके नाम या प्रतीक में नाग का प्रभाव देखा जा सकता है।उड़ीसा के मंदिरों, विशेषकर कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में सर्पों और नाग-नागिनियों के चित्रण मिलते हैं, जो उनके धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। ओडिशा की लोककथाओं और आदिवासी परंपराओं में भी नागों का महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड (बिहार का दक्षिणी भाग): नागवंशी शासकों का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें फणीमुकुट राय जैसे राजाओं ने सदियों तक शासन किया। बंगाल और उड़ीसा क्षेत्रों में नागों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक रहा है, खासकर देवी मनसा की पूजा और कलात्मक चित्रणों में राजवंशों के साथ नागों के प्रतीकात्मक संबंध हैं । सनातन धर्म संस्कृति में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, अनंत और अन्य आदि नागों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल सर्प नहीं, बल्कि दिव्य सत्ताएँ, ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक और शक्तिशाली वंशों के मूल माने जाते हैं। इनके शासन और वंशजों के बारे में विभिन्न पुराणों और लोककथाओं में विस्तृत वर्णन मिलता है।
शेषनाग (अनंत) - शेषनाग को सभी नागों में ज्येष्ठ, सबसे शक्तिशाली और परम ज्ञानी माना जाता है। उन्हें 'अनंत' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और क्षीरसागर में उनकी शैया के रूप में विराजते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है, जो ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक है। शेषनाग का शासन प्रत्यक्ष रूप से किसी भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि संपूर्ण पाताल लोक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर माना जाता है। वे नागलोक के अधिपति और समस्त नागों के राजा हैं।पुराणों के अनुसार, शेषनाग ने भगवान विष्णु के अवतारों की सेवा में धरती पर अवतार लिया है। लक्ष्मण: भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम: भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों और सिक्कों के आधार पर, यह भी माना जाता है कि शेषनाग ऐतिहासिक राजा था जिसने 110 ईसा पूर्व में विदिशा (मध्य प्रदेश) को राजधानी बनाकर शेषनाग वंश की नींव रखी। इनके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए। इस वंश के कुल मिलाकर पांच राजाओं ने लगभग 80 वर्षों तक शासन किया।
वासुकी - वासुकी नागों के दूसरे सबसे प्रमुख राजा और शेषनाग के बाद ज्येष्ठ भ्राता माने जाते हैं। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनके गले का आभूषण हैं। वासुकी को नागलोक का राजा है। शेषावतार लक्ष्मण मंदिर उत्तराखण्ड राज्य का हेमकुंड में स्थित है। पुराणों के अनुसार, वासुकी का कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में राज्य था। वे नागलोक के शासकों में से एक थे। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी को नेती (रस्सी) के रूप में प्रयोग किया गया था।
त्रिपुरदाह: त्रिपुरदाह के समय वे भगवान शिव के धनुष की डोर बने थे।वासुकी का सीधा वंशज किसी ऐतिहासिक राजवंश के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन वे स्वयं नागों के एक प्रमुख कुल के संस्थापक माने जाते हैं। हाल ही में गुजरात में 'वासुकी इंडिकस' विशालकाय सांप के जीवाश्म मिलने से भी इस नाम से जुड़ी प्राचीनता और विशालता को बल मिलता है। झारखण्ड राज्य के दुमका जिले का जरमुंडी प्रखण्ड का वासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में में नागराज वासुकी द्वारा स्थापित बाबा वासुकीनाथ शिवलिंग है।
तक्षक - महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्षप्रजापति की पुत्री कद्रू के पुत्र तक्षक शक्तिशाली नाग राजा हैं।
तक्षक का राज तक्षशिला में था, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तक्षशिला (वर्तमान पाकिस्तान में) एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर था, जो तक्षक नाग के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। द्वापरयुग में राजा परीक्षित की मृत्यु: तक्षक नाग ने श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित को डँसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी । राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्पयज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें हजारों नाग भस्म हो रहे थे। तक्षक भी इस यज्ञ में आहुति बनने वाले थे, लेकिन ऋषि आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप कर यज्ञ को रुकवाया और नागों की रक्षा की। तक्षक को अपने कुल का संस्थापक माना जाता है, जिससे तक्षक कुल के नाग उत्पन्न हुए। में विभिन्न संख्या में आदि नागों का उल्लेख मिलता है। ये आठ या बारह या चौदह प्रमुख नागों के रूप में जाने जाते हैं, जो नागलोक के आधार स्तंभ और विभिन्न क्षेत्रों के संरक्षक माने जाते हैं। ये सभी महर्षि कश्यप और कद्रू के पुत्र हैं। शेष (अनंत) , वासुकी , तक्षक , पद्म , महापद्म , शंख , कुलिक ,कर्कोटक , धृतराष्ट्र , कंबल , अश्वतर , कालिया ,पिंगला , धनंजय आदि नागों को नागलोक के विभिन्न हिस्सों का स्वामी और संरक्षक माना जाता है। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कालिया नाग का यमुना नदी पर शासन था जिसे भगवान कृष्ण ने विनियमित किया।ऐतिहासिक राजवंशों से संबंध: पुराणों के अनुसार, एक समय ऐसा था जब नागा समुदाय पूरे भारत (वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित) के शासक थे।विदिशा, कांतिपुरी, मथुरा, और पद्मावती (पवाया): इन क्षेत्रों में नागवंशी राजाओं का शासन रहा है। विष्णुपुराण में 'नवनागों' का उल्लेख है जिन्होंने इन स्थानों से शासन किया।मध्य प्रदेश: पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नाग वंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदि, शिशुनंदि या यशनंदि आदि का उल्लेख मिलता है।झारखंड: जैसा कि पहले बताया गया है, झारखंड के नागवंशी शासक (जैसे फणीमुकुट राय) स्वयं को नागों के वंशज मानते थे।अन्य क्षेत्र: भारत के कई हिस्सों में 'नाग' शब्द पर आधारित शहर और गांव मिलते हैं, जो नागों की व्यापक उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाते हैं।नागवंशियों की विविधता: नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग शामिल थे, जो दर्शाता है कि यह एक व्यापक और विविध समूह था । शेषनाग, वासुकी, तक्षक और अन्य आदि नाग भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे न केवल दिव्य प्राणी हैं बल्कि ब्रह्मांडीय कार्यों में भी संलग्न हैं। जबकि उनके पौराणिक 'शासन' का संबंध नागलोक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से है, वहीं उनके नाम और प्रभाव से प्रेरित कई ऐतिहासिक नागवंशी राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया है। ये राजवंश नागों को अपने पूर्वज या संरक्षक देवता के रूप में पूजते थे, जिससे उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान नागों से जुडा है। करपी , अरवल , बिहार 804419
हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews #Divya Rashmi News, #दिव्य रश्मि न्यूज़ https://www.facebook.com/divyarashmimag




%20(1).jpg)
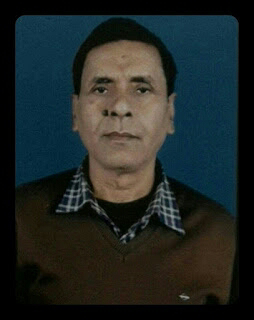

0 टिप्पणियाँ
दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |
खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com