पंचतंत्र के रंगे सियार और फास्टफूड शिक्षा
देहरादून स्थित शैमरॉक प्री-स्कूल में मैने अपने बेटे का प्रवेश कराया था। प्री-स्कूल का अर्थ क्या है? विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा खेले-कूदे, हमउम्र बच्चों के बीच मिले-जुले और इस तरह जो सिखाया जा सकता है उसी माध्यम से उसकी बुनियाद इस तरह गढी जाये कि अध्ययन में अभिरुचि हो। इसके ठीक उलट मुझे डायरी में बार बार नोट मिलते कि पालक ध्यान दें, बच्चा याद नहीं कर रहा है या कि स्कूल में आ कर मिलें। मैंने हाजिरी लगाई तो वही रोना फाईव फ्लावर याद नहीं हैं, फाईव एनिमल नहीं बोल पाता, फाईव प्लांन्ट्स के नाम याद कराईये। मैं देख रहा हूँ कि बस्ता भारी वाली पीढी बढती ही जा रही है। ये कैसे प्ले स्कूल हैं और कैसे खेल खिला रहे हैं? बच्चा प्लांट की जगह पौधा समझे तो क्या दिक्कत? नयी पीढी से मुझे सहानुभूति है जिसे इस तरह पीसा जा रहा है मानो ब्लैक लैटर्स नहीं बफैल्लो हो। हमारे देश का ब्लैकबोर्ड ही ब्लैकआउट हो चुका है और हम गुमान में हैं कि कुछ सिखा-पढा रहे हैं। बच्चे की हिन्दी और अंग्रेजी विषयक किताबें पलटकर देखता हूँ तो कुछ जाना-पहचाना प्रतीत होता है। अंग्रेजी या कि हिन्दी की पाठ्य पुस्तक मे जो भी कहानियाँ हैं, सभी पंचतंत्र का ही विकृत अनुवाद भर तो है? नया क्या है? दो-ढाई हजार साल पुरानी सामग्री है यह जिसे मॉडर्न एज्यूकेशन के नाम पर रिमॉडल किया गया है। हमें क्या? बच्चा ऐसे नामी-गिरामी स्कूल में पढ रहा है न जिससे कि स्टेटस सिम्बल बनता हो? हम शिक्षा जगत के उन रंगे सियारों को अब भी नहीं पहचानते जिन्होने हमारे बच्चों को ट्विंकल-ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम बाईहार्ट करा दिया है। सत्तर साल पहले ही अंग्रेज भारत से गये, अब तो मैकाले को कंधे से उतारा जाये?
पंचतंत्र से कौन परिचित नहीं? आज भी रचा जा रहा अधिकांश देसी-विदेशी बाल साहित्य पंचतंत्र की ही नकल है अथवा उससे प्रभावित। क्या वैदिक ज्ञान-परम्परा का विस्तार यह ग्रंथ बालक-शिक्षा किस तरह दी जा सकती है उसका श्रेष्ठतम उदाहरण नहीं है? बात भी लगभग 300 ईसा पूर्व की है। कहते हैं कि दक्षिण भारत में कहीं महिलारोप्य नाम का राज्य था जिसके राजा थे अमरशक्ति। दक्षिण भारत शब्द को दोहरा कर पढियेगा जिससे आपका यह पूर्वाग्रह कुछ हद तक मिटे कि ज्ञान के कतिपय उत्तर भारतीय केंद्र भर नहीं थे अपितु समस्त जम्बूदीप का अपने अपने तौर से योगदान रहा है। राजा के तीन बेटे थे - बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंतशक्ति जो न केवल अहंकारी अपितु विद्या ग्रहण करने की ओर से उदासीन थे। राजा ने बहुत चेष्टा की लेकिन कोई पढना ही न चाहे तो कैसे पढाया जाये? यह सवाल ठीक इसी तरह आज भी सामने है, इसका उत्तर आधुनिक शिक्षकों के पास है कि पालकों को बुला कर जलील कर लो, बच्चे को कक्षा में हतोत्साहित कर दो, वगैरह वगैरह। क्या पढाया जाना चाहिये क्या इससे अधिक महत्वपूर्ण यह नहीं कि कैसे पढाया जाना चाहिये? राजा अमरशक्ति को सुझाया गया कि राज्य में विद्वान विष्णु शर्मा हैं जिनसे सहायता ली जा सकती है। राजा तो राजा है उसने विष्णु शर्मा को बुलवाया और सीधे ही सौदेबाजी कर डाली। सौ गाँव आपको दे दूंगा अगर राजकुमारों को आपने योग्य बन दिया। राजा ने प्रस्ताव दिया लेकिन शिक्षक तो फक्कड था। विद्यार्थी ले लिये, धन छोड दिया। क्यों पोथे-किताबें दिखा कर डराना? विष्णु शर्मा ने किस्सागोई का सहारा लिया। जो कुछ सिखाना था वह रोचक कहानियों में ढल गया। अब शास्त्र नहीं थे, सूत्र नहीं थे, प्रमेय नहीं थे अपितु शैतान बंदर था, चालाक लोमडी थी, दुष्ट भेडिया था मासूम मेमना था। जीवजगत के ये किरदार, नीति की वे शिक्षायें बन गये जो इस सृष्टि के रहने तक प्रासंगिक रहेंगी।
पाँच तंत्रों अथवा भाग में पंचतंत्र की कहानियाँ संकलित हैं – मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि-विग्रह/काकोलूकियम (कौवे एवं उल्लुओं की कहानियाँ), लब्ध प्रणाश एवं अपरीक्षित कारक। मित्र कैसे होने चाहिये, मित्रता का लाभ क्या है, यदि आप किसी संकट में हैं तो उससे बाहर आने का रास्ता क्या है, किसी कार्य को करने से पूर्व क्या करें, कैसे परख करें आदि जैसे विषयों के माध्यम से प्राचीन पंचतंत्र ग्रंथ प्राथमिक शिक्षा का जांचा-परखा सर्वयुगीन सिलेबस है। विष्णु शर्मा के पास बीएड नहीं था। पढाने का कोई सरकारी प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था। वे न तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे न ही जेएनयू से पीएचडी। वे अलग थे, बिलकुल मौलिक। उन्होंने संस्थानों को रास्ता दिखाया है कि प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जानी चाहिये। यह अलग बात है कि आज के स्कूली पाठ्यक्रमों ने उनकी नकल तो की लेकिन थोथा-थोथा भर, सार-सार को तो उडा दिया।
कितने प्रतिशत भारतीय जानते हैं कि सचिन तेंदूलकर क्रिकेट के महानतम खिलाडी हैं? इस प्रश्न का उत्तर सौ बटा सौ मिल जायेगा लेकिन क्या हम भारत के लोग यह जानते हैं कि बाईबल के बाद दुनिया का सबसे अधिक प्रसार प्राप्त ग्रंथ है - पंचतंत्र। वह दुनिया की अभागी भाषा ही होगी यदि उसके पास पंचतंत्र का अनुवाद उपलब्ध नहीं है। विदेशी भाषा में पंचतंत्र का पहला ज्ञात अनुवाद 570 ई. में सिरियाई भाषा में हुआ था। लगभग 750 ई. में सीरियाई भाषा से अरबी में अब्दुल्ला इब्नल मोकफ्फा के प्रयासों से अनूदित हुआ। इसके पश्चात लगभग दसवी-ग्यारहवी सदी के अगमन तक यूरोप में पंचतंत्र अपनी पैठ जमाने लगा। यूनानी (ग्यारहवी सदी), हिबू्र (ग्यारहवी सदी), लैटिन (1263 से 1278 के मध्य), फारसी (1470 से 1505 के मध्य), जर्मन (1483), स्पेनिश (1493), इटालियन (1546), फ्रेंच (1556 तथा 1644), अंग्रेजी (1570) तथा इतालवी (1583) आदि पंचतंत्र के आरम्भिक विदेशी भाषा में किये गये अनुवाद थे। अनेक समकालीन अथवा बाद के भारतीय ग्रंथ भी पंचतंत्र की आभा में लिखे गये इनमें प्रमुखता से गिने जाते हैं - तन्त्राख्यायिका, दक्षिण भारतीय पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र, हितोपदेश, सोमदेव कृत कथासरित्सागर, क्षेमेन्द्र कृत बृहत्कथा-मंजरी, पश्चिमी भारतीय पंचतंत्र, पूर्णभद्र कृत पंचाख्यान आदि।
पंचतंत्र को आज बाल-साहित्य की तरह देखा परखा जाता है जबकि आवश्यकता इसकी रचनाप्रक्रिया और उसके उद्देश्य को समझने की है। विष्णु शर्मा ने राजा से उसके पुत्रों को शिक्षा देना स्वीकार किया तब कहा – “किंतु त्वत्प्रार्थना सिद्धयर्थे सरस्वती विनोद करिष्यामि”। सरस्वती विनोद शब्द पर ध्यान दीजिये। क्या विनोद-आनंद के साथ सरस्वती प्रदान करने का तरीका नहीं है पंचतंत्र? विषय कितना भी जटिल हो क्या उसे सरल तरीके से समझाने का तरीका पंचतंत्र में अंतर्निहित नहीं है? साथ ही फाईव एनिमल रटाने वाले अध्यापक ध्यान दें कि केवल पंचतंत्र को ही “सरस्वती विनोद” पूर्वक बताते रहने पर आपका विद्यार्थी जाने कितने एनिमल, कितने ही बर्ड, कितने ही प्लांट वगैरह वगैरह के नाम ही नहीं जान सकेगा अपितु उसके माध्यम से उसे वे नैतिक शिक्षायें भी प्राप्त होंगी जो आज के फास्ट-फूड सिलेबस में कहीं पीछे छूट गयी हैं।
विश्व के आश्चर्यों की गिनती करने वालों के हिसाब में एलोरा का कैलाशमंदिर सम्मिलित नहीं मिलेगा। आप इतिहास के ग्रंथ उठा लीजिये, केवल इतना पायेंगे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से अठ्ठाईस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा की विश्वप्रसिद्ध गुफायें जिन्हें स्थानीय भाषा में वेरूल लेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसी गुफाश्रृंखला की एक कडी है भगवान शिव को समर्पित कैलाशमंदिर। मंदिर के आलेखन का कार्य राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग (735 – 757 ई.) द्वारा किया गया तथा निर्माण का श्रेय राजा कृष्ण प्रथम (757-773 ई.) को जाता है। अभियांत्रिकी की कोई पुस्तक उठा लीजिये आपको उल्लेख यही मिलेगा कि बुनियाद पहले बनायी जानी चाहिये और उसके उपर खड़ा किया जायेगा भवन। भारत के कितने अभियंता यह जानते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस विधि अथवा प्रक्रिया से हुआ है? बुनियाद तैयार करने के पश्चात तो बड़े बड़े भवन खड़े किये जाते हैं लेकिन अद्भुत शिल्पी थे वे जिन्होंने पहले शीर्ष पर काम आरम्भ किया। एक सिरे से भीतरी भाग का उत्खनन किया जाता रहा है जिससे हजारो टन पत्थर के पृथकीकरण के पश्चात केवल मंदिर ही शेष रह गया। धीरे धीरे शिल्पियों के छेनी-हथौडों ने बुनियाद रचने के पश्चात विराम लिया। एक पर्वताकार बेसाल्टिक शिला के लगभग पिच्यासी हजार क्यूबिक मीटर हिस्से में से काट-तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। देखा जाये तो भू-वैज्ञानिकों के लिये भी यह मंदिर एक प्रयोग शाला बन सकता है। कैलाश मंदिर मुख्य रूप से बेसाल्ट की चट्टानों को काट कर बनाया गया है। बेसाल्ट वस्तुत: एक दौर में विभिन्न चरणों ने उत्सर्जित लावा प्रवाह के कारण निर्मित चट्टाने हैं जो प्रवाह के विभिन्न दौर में सीढीनुमा आकार ले लेती हैं। एलोरा के निकट कोई भू-विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति उन दरारों (गुफा क्रमांक 32 के निकट) को भी देख-परख सकता है जिनसे हो कर कभी लावा प्रवाहित हुआ करता था। बेसाल्ट चट्टानों से अटी पड़ी ये पहाड़ियाँ वस्तुत: सह्याद्रि पर्वत माला का हिस्साो हैं जिनका निर्मिति काल क्रिटेशियस युग (लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व) माना गया है। बेसाल्ट चट्टानें उस दौर में मूर्तिकला के लिये श्रेष्ठतम मानी जाती थीं।
इनकार नहीं कि जॉन स्मीटॉम (18वी सदी) को अभियांत्रिकी का पिता कहा जाये परंतु पितामहों की सुध कौन लेगा? एलोरा समूह की गुफा क्रमांक -16 को कैलाशनाथ मंदिर के रूप में पहचान मिली है। गुफा श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ तथा सुन्दरतम गुफा मंदिर है कैलाश, जो भारत में ज्ञात चट्टान काट कर बनाये गये मंदिरों में विशालतम है। कैलाशमंदिर को बनाने में दस पीढियाँ और लगभग दो सौ साल का समय लगा है यह दर्शाता है कि कितना धैर्य, कितनी योजना और कितना श्रम इस निर्माण के पीछे है। आज जब हम विशालकाय मशीनो और उन्नत अभियांत्रिकी के दौर में रह रहे हैं तब भी निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अब कैलाशनाथ मंदिर जैसी संरचना का पुनर्निर्माण असम्भव है। इस विषय को विस्तार देने से पूर्व कैलाश गुफा मंदिर को समग्रता से विवेचित करते हैं। मंदिर का प्रवेशद्वार लगभग पचास मीटर लम्बा तथा तैंतीस मीटर चौड़ा है। प्रवेश करते ही दो मुख्य महाकाव्य रचयिता संत क्रमश: वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी तथा वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्हें प्रदर्शित किया गया है। द्वार मण्डप पर अवस्थित चार स्तम्भ में कलश व पत्ते वस्तुत: समृद्धि व उर्वरता के प्रतीक के रूप में स्थापित किये गये हैं। द्वारमार्ग के दोनो और कुबेर के चित्र उकेरे गये है जो समृद्धि के प्रतीक है। स्वागत द्वार के दो और मुख्य आकर्षण हैं गणेश तथा दुर्गा की भव्य प्रतिमायें। प्रवेश के पश्चात दाहिनी और की दीवार पर स्तम्भों के पार्श्व में गंगा यमुना तथा सरस्वाती नदियों की प्रतिमायें हैं। प्रत्येक नदी को स्त्रीरूप में अपने वाहन अर्थात गंगा मगरमच्छ पर, यमुना कछुवे पर तथा सरस्वती को हाथी पर दर्शाया गया है, जो कि सांकेतिक रूप से शुद्धता, समर्पण तथा प्रज्ञता के प्रतीक हैं। प्रवेशद्वार पर उत्कीर्णित शंखनिधि, पद्मनिधि तथा गजलक्ष्मी राज्य के वैभव सम्पदा की साक्षी है।
मंदिर का विमान एक समानांतर चतुर्भुज के आकार का है तथा उसे पच्चीस फीट ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर में एक सीढी बनी हुई है जिससे ऊपर बरामदे तक पहुँचा जा सकता है। मंदिर का शिखर पन्चानबे फीट ऊँचा है। मंदिर के प्रधान भवन में एक गर्भगृह है, जिसके आगे स्तम्भ युक्त मण्डप निर्मित है। मंदिर के चारो ओर बरामदे, स्तम्भ, पंक्तियाँ तथा कमरे निर्मित हैं। मंदिर भीतर बाहर चारों ओर मूर्ति-अलंकरणों से भरा हुआ है। मुख्य भवन के पश्चात एक नंदि मंदिर निर्मित है जिसके दोनो और दो ध्वज स्तभ हैं और उनपर त्रिशूल स्थापित किये गये हैं। खुले मंडप में नंदि है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। मुख्यमण्डप, नंदिमंडप, प्रवेशद्वार, गलियारा, बरामदा, तथा गौण मंदिर आदि इस संरचना के प्रमुख अंग हैं। सम्पूर्ण रचना में ताख, स्तम्भ, अर्धस्तम्भ, गवाक्ष के साथ नखशिखांत अलंकृत हैं। प्रमुख अलंकरण में देवी देवताओं की विशाल प्रतिमायें, पुराण महाकाव्य दृश्य, मिथुन मूर्तियाँ, पशु-पक्षी, बेल-बूटियाँ तथा ज्यामितीय अलंकरण का समावेश है। उत्कीर्ण पश्चात मंदिर को बार बार चित्रित किया गया था। मुख्य मंदिर तो सम्पूर्ण रूप से चित्रित था इसी लिये इसे रंगनाथ रंगमहल भी कहा जाता है। रंगमहल का सात मीटर ऊँचा आधार तल ठोस और अनुप्रयोग्य है जो विशालकाय हाथी, सिंह, काल्पनिक पशु तहा रामायण महाभारत के दृश्यों से अलंकृत है। मंदिर एक बहुत बड़े आँगन के केन्द्र में स्थित है जिसे खम्बों और विशालकाय उत्कीर्णित हाथियों का सहारा दिया गया है। इससे ऐसा आभास होता है कि यह मंदिर अधर में लटका हुआ है। मंदिर विन्यास में मुख्यत: वाद्यमण्डप, नंदीमण्डप, नाट्यमण्डप, अर्धमण्डप, स्तम्भयुक्त मण्डप, अंतराल, पूजागृह, गलियारा, गौणमंदिर आदि का समावेश है। गर्भगृह, अंतराल, मंडप की छतों पर विकसित कमल, अन्नपूर्णादेवी तथा नटराजशिव का अनुक्रम अंकन है।
सम्पूर्ण मंदिर तीनो ओर से स्तम्भयुक्त गलियारे से घिरा है जहाँ हिन्दू पौराणिक मूर्तियों का उत्कीर्णन है। प्रांगण स्थित उत्तुंग कीर्ति स्तम्भ शैव धर्म का प्रभाव एवं विशाल गजराज राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को प्रदर्शित करता है। उत्तरी गलियारे में लंकेश्वर मंदिर की रचना की गयी है। मंदिर विन्यास में मंडप, अंतराल, गर्भगृह, नंडीमण्डप आदि का समावेश है। मंदिर के आधार भाग में पशु पक्षियों की पंक्तियों के उपर मिथुन मूर्तियों का पट्ट भी उत्कीर्णित है। मंदिर के स्तम्भ व दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्णित हैं पूजागृह में भग्न शिवलिंग तथा पार्श्विक दीवार पर महेशमूर्ति का अंकन है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का स्वरूप देने में भी शिल्पकारों ने कोई कमी नहीं की थी अपितु मंदिर के शीर्ष पर स्थित पत्थरों को सफेद प्लास्टर व रंग के प्रयोग से हिमाच्छादित दर्शाया गया था। समय के साथ मंदिर पर की गयी चित्रकारी के रंग उतर गये हैं अथवा कई प्रतिमायें खण्डित हो गयी हैं तथापि कैलाशमंदिर अब भी शान से मुस्कुराता हुआ सिर उठाये खड़ा है। संरचना की पिछली ओर से पहाड़ी टीले पर चढ़ कर शीर्ष से यदि मंदिर को देखा जाये तो इसका वास्तविक वैभव दृष्टिगोचर होता है। छत को इस तरह सजाया-संवारा गया है कि दूर से देखने पर ही इस स्थल की अनुपमता का अहसास होने लगे। यह ठीक है कि युनेस्को ने एलोरा गुफा समूहों को विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया है किंतु क्या कैलाश गुफा मंदिर को केवल इतना ही महत्व प्राप्त होना चाहिये? क्या कैलाश मंदिर प्राचीन अभियांत्रिकी का आज भी संरक्षित उदाहरण नहीं है?
हमने या हमारी पाठ्यपुस्तकों ने इससे क्या सीखा? भारतवर्ष जहाँ सैंकडो ग्रंथ केवल भवन-निर्माण, वास्तुशास्त्र आदि पर केंद्रित हैं वे हमारी वर्तमान समझ को क्या अवदान दे रहे हैं? इस प्रश्न को थोडा बदल कर फिर सामने रखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तुशास्त्र के उपलब्ध ज्ञान का क्या उपयोग कर रही है? कुछ वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ जैसे अपराजितपृच्छा, कर्णागम, प्रासादमण्डन, राजवल्लभ, वास्तुसौख्यम्, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, सनत्कुमारवास्तुशास्त्र, वास्तुमण्डन, मयशास्त्र, शुक्रनीति, वास्तुविद्या, प्रतिमालक्षणविधानम्, मानसार शिल्पशास्त्र, मयमतम्, बृहत्संहिता, शिल्परत्नम्, समरांगणसूत्रधार, वास्तुकर्मप्रकाशम्, विश्वकर्मा शिल्प, अगत्स्य, उपवन विनोद, वास्तुसूत्र आदि को क्या केवल शोभा की वस्तु नहीं बना दिया गया है? क्या यह सत्यता नहीं कि आज की अभियांत्रिकी को दंभ है कि वह आधुनिकता के सर्वोच्च पायदान पर है, फिर भी कोई दूसरा ताजमहल अब तक नहीं बनाया जा सका? क्या यह सच नहीं कि अब कैलाशमंदिर जैसा कोई भवन निर्मित किया जाना कल्पना से परे है? क्या यह सच नहीं कि अब भारत में जो इमारतें बनाई जा रही हैं उनमें भारतीयता का संपुट नहीं के बराबर है? सीमेंट और कंकरीट का जंगल बनता जा रहा है लेकिन कहाँ हैं वह कलात्मकता जो हमारी पहचान हुआ करती थी? हम फ्यूजन के दौर में रह रहे हैं फिर हमारी इंजीनियरिंग की शिक्षा संस्थानों को कुछ पुराने पन्ने भी उद्धरित कर लेने में समस्या क्या है? हर समय को निर्माण शैली से पहचान मिली है लेकिन हमारा तो नकल युग है। अपना ही प्राचीन ज्ञान यदि आपके अध्ययन-अध्यापन का हिस्सा नहीं तो हसिल ठन-ठन गोपाल होना है।
दिव्य रश्मि केवल समाचार पोर्टल ही नहीं समाज का दर्पण है |www.divyarashmi.com




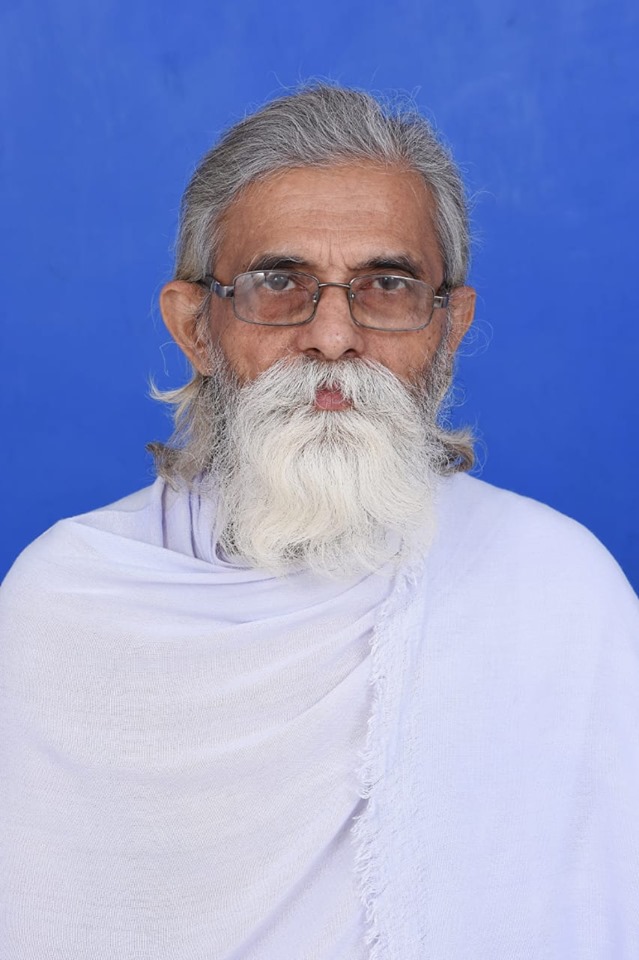


0 टिप्पणियाँ
दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |
खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com